
हाल के दिनों में सीबीएसई अपने सिलेबस में बदलाव को लेकर बहुत सुर्ख़ियों में रहा हैं। सिलेबस में इतिहास सम्बन्धी विषयों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश के साथ ही इनमें बदलाव भी हो रहे हैं। लेकिन विमर्शों से जुड़े विषयों का क्या? ख़ासकर पाठ्यक्रम में स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दे? कोरोना काल में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई जा रही दो कविताओं पर ऑनलाइन आपत्ति तो जताई गई लेकिन फ़िर उनका क्या हुआ?
केजी में बहुत ज़ोर-शोर से रटाई जाने वाली एक कविता विवादों में थी जो समाज द्वारा निर्धारित जेंडर्ड रोल्स को नॉर्मलाइज़ करती है। कविता की पंक्तियाॅं- “मम्मी की रोटी गोल-गोल, पापा के पैसे गोल-गोल” कैसे छोटे बच्चों के अवचेतन मन को ये समझाते हैं कि घर में पैसे केवल पिता(पुरुष) कमाता है और मम्मी(स्त्री) का दायरा रसोई तक सीमित है।
प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली एक और कविता ‘आम की टोकरी’ विवादों में घिरी थी जिस पर बाल श्रम को प्रोत्साहन देने के साथ ही द्विअर्थी होने का आक्षेप लगाया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने इसे ये कहकर डिफेंड किया कि द्विअर्थी इसे आप समझ रहें हैं न कि 5-6 वर्षीय बच्चे। वहीं इस विवाद पर हिन्दी की सुप्रसिद्ध रचनाकार ममता कालिया का कहना था कि- “ये एक ख़राब रचना का उदाहरण है। बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक कविताएँ एकतारा और तक्षिला प्रकाशन के पास है। नरेश सक्सेना, स्वयंप्रकाश और अनिरुद्ध उमट ने बच्चों की बेहद दिलचस्प कविताएँ लिखी हैं। पाठ्यक्रम समिति में जानकार लोग हों तभी सही काम हो सकता है।”
अब विश्वविद्यालयों का ही हाल देख लीजिए। सीबीसीएस बोर्ड के हिन्दी स्नातक में एक ओर बच्चे स्त्री विमर्श पढ़ते हैं तो वहीं दूसरी ओर नारी को विधाता की निम्तर सृष्टि और नर को आकर्षक, सबसे सुन्दर और गुणवान बताने वाला ‘रस आखेटक’ शीर्षक से कुबेरनाथ राय का ललित निबंध पढ़ते हैं।
इस निबंध की विषय-वस्तु कुछ और है जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है लेकिन विषय से भटककर बीच में इस तरह की टिप्पणी लिखने का लेखक का औचित्य समझ नहीं आता है। वो भी पाठक को विश्वास दिलाने के लिए विस्तार से (क़रीब 400 शब्दों में) अलग-अलग उदाहरणों से समझाते हैं। भारतीय शिल्पकला में हिन्दू बौद्ध मूर्तिकला व अजंता के प्रसिद्ध चित्र आदि का उदाहरण देकर वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि- “सृष्टि में यदि गौर से देखा जाए तो सर्वत्र नर ही सुन्दर और गुणवान है, नारी में सृजन सामर्थ्य मात्र है और कुछ नहीं।”
ख़ैर उनका यह व्यक्तिगत विचार है और लेखक अपने विचार लिखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हैरत इस बात पर होती है कि पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाली समिति ने इसको किस आधार पर पाठ्यक्रम में शामिल किया है? यदि यह शिक्षक की समझ और सूझबूझ पर छोड़ा गया है तो यहाॅं यह समझना ज़रूरी है कि शिक्षक की जेंडर अवधारणा से हम परिचित नहीं है कि इस बारे में उनकी समझ क्या है। सच कहा जाए तो सारे शिक्षक भी जेंडर पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होते।
कुछ आगे बढ़कर देखें तो यह पाठ्यक्रम के उदाहरणों में भी देखने को मिलता है। हालाॅंकि पाठ्यक्रम समिति की इतनी कोशिशों के बाद भी कमियाॅं अब तक मौजूद है।
7वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की किताब का एक उदाहरण याद आ रहा है, जिसमें सबको समान मतदान अधिकार के बावजूद सामाजिक वर्ग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समझाने की कोशिश की गई है।
उदाहरण में महिला ही सारी भूमिकाओं में नज़र आती है, चाहे घर पर बीमार बेटी की देखभाल करना हो या बाहर किसी के घर पर काम करके पैसे कमाना हो। ऐसा उदाहरण जहाॅं सब रोल स्त्री के पास है। लेकिन यहाॅं पुरुष कहाॅं है? वो किसी भी भूमिका में नहीं है। न ही ऐसा कुछ मेंशन किया किया गया है कि वो स्त्री एक सिंगल मदर है। ऐसे में उसे आज की “टिपिकल आइडियल वुमन” जैसा दिखाने के पीछे क्या सोच रही होगी ये समझ पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। बेशक मेरा संकेत सामाजिक अनुकूलन की तरफ़ है। हालाॅंकि इसी किताब में आगे लैंगिक समानता पर पूरा एक अध्याय समर्पित है। तब हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं।
स्कूली बच्चों और विमर्शों की दुनिया के बीच यों तो फासला कम नहीं। लेकिन जब विमर्शों की चर्चा होती है तब पाठ्यक्रम के नाम पर क्या परोसते हैं?
स्कूल या शिक्षण संस्थान सामाजिक अनुकूलन में सहायक है लेकिन फ़िर भी हम मानते हैं कि अगर बच्चे, ख़ासकर लड़कियाॅं पढ़-लिख जाएँगी तो समाज की बनाई अपनी सीमित भूमिकाओं से बाहर निकल, ख़ुदको एक इन्सान के रूप में देखे सकेंगी और हक़ से अपने हक़ की बात भी कहेंगी। लेकिन जब पाठ्यक्रम ही ऐसे अनुकूलन का टूल हो तब?

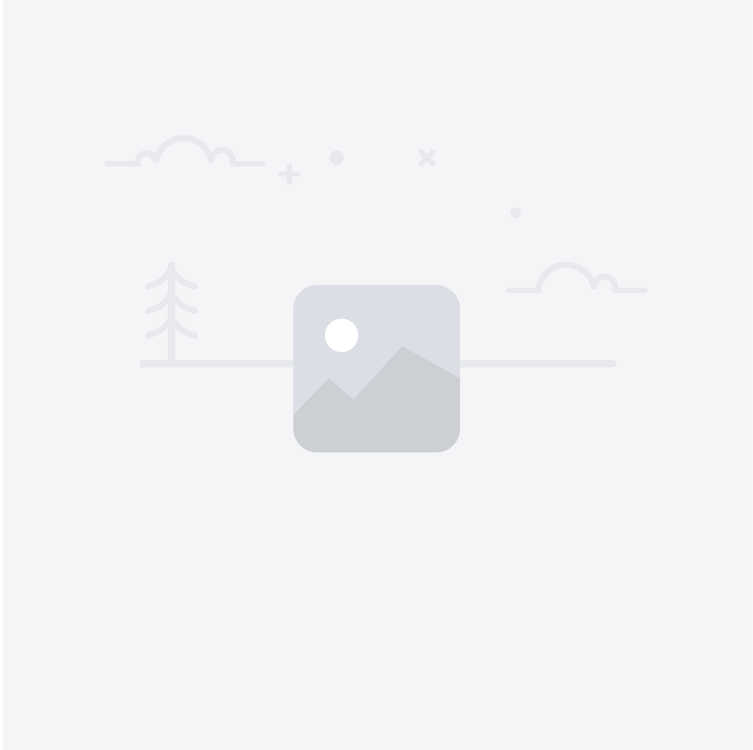












Write a comment ...